Talking Point
ट्रीटेक नेटवर्क
आईआईटी बॉम्बे और सस्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत ने 2015 और 2019 के बीच प्राप्त किए गए वन क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक वन क्षेत्र खो दिया। अध्ययन में पाया गया कि प्राप्त प्रत्येक एक वर्ग किलोमीटर वन के लिए, देश ने लगभग 18 वर्ग किलोमीटर खो दिया। यह खतरनाक अनुपात भारत में वन विखंडन की एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करता है। अध्ययन, जिसमें कोपरनिकस ग्लोबल लैंड सर्विस लैंड कवर मैप से डिजिटल वन कवर मैप्स का उपयोग किया गया था, निर्दिष्ट अवधि के दौरान सभी राज्यों में वन कवर के शुद्ध नुकसान को इंगित करता है।
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक नुकसान वाले राज्यों के रूप में पहचाना गया, जो कुल गिरावट के लगभग आधे हिस्से में योगदान करते हैं। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि हालांकि वन कवर में कुछ लाभ देखा गया था, ये बड़े पैमाने पर छोटे, अलग-थलग पैच थे जो पारिस्थितिक संपर्क में योगदान नहीं करते थे। इसके विपरीत, नुकसान में मुख्य रूप से बड़े, निरंतर वन क्षेत्र शामिल थे। यह दीर्घकालिक स्थिरता और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वन कार्बन पृथक्करण और जल विनियमन जैसे अपने महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। अध्ययन के निष्कर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण की पिछली रिपोर्टों से भी भिन्न हैं, जिनमें अक्सर वन आवरण में समग्र वृद्धि का संकेत दिया गया है।
अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित कारणों का हवाला देते हैंः असमान हानिः अध्ययन में पाया गया कि भारत ने 2015 और 2019 के बीच प्राप्त प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर के लिए 18 वर्ग किलोमीटर वन खो दिया। ऽ शुद्ध हानिः इस अवधि के दौरान भारत के सभी राज्यों में वन आवरण का शुद्ध नुकसान हुआ। ऽ खंडित लाभः वन आवरण में वृद्धि अक्सर खंडित ‘‘द्वीपों‘‘ में हुई, जो बड़े वन क्षेत्रों की तुलना में पारिस्थितिक रूप से कम मूल्यवान हैं। ऽ आधिकारिक रिपोर्टों में अंतरः अध्ययन के परिणाम उन आधिकारिक रिपोर्टों से भिन्न हैं जो वन आवरण में वृद्धि दर्शाती हैं, मुख्यतः पद्धतिगत अंतर के कारण। ऽ संरचनात्मक संपर्क का महत्वः शोधकर्ताओं ने पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और वन्यजीवों के लिए वन गुणवत्ता और संपर्क के महत्व पर प्रकाश डाला। ऽ नीतिगत सुझावः यह अध्ययन संरचनात्मक संपर्क और पारिस्थितिक लचीलेपन में सुधार पर केंद्रित वन नियोजन के लिए एक नए ढाँचे का सुझाव देता है। अध्ययन में कहा गया है, ‘‘हालाँकि भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) और अन्य स्वतंत्र अध्ययन नियमित रूप से भारत के सकल वन क्षेत्र पर रिपोर्ट देते हैं, फिर भी देश भर में संरचनात्मक संपर्क को समझने और वन विखंडन की निगरानी के लिए अभी तक कोई व्यवस्थित ढाँचा नहीं बना है।‘‘
आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर राज रामशंकरन और सस्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी के डॉ. वासु सत्यकुमार और श्रीधरन गौतम के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में कोपरनिकस ग्लोबल लैंड सर्विस (सीजीएलएस) लैंड कवर मैप से प्राप्त वन आवरण आँकड़ों पर मॉर्फोलॉजिकल स्पैटियल पैटर्न एनालिसिस (एमएसपीए) का प्रयोग किया गया। यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उपग्रह आँकड़ों और ओपन-सोर्स टूल्स का उपयोग करके भारत में वन विखंडन का पहला देश-स्तरीय आकलन प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन की एक मुख्य विशेषता वनों को सात संरचनात्मक प्रकारों में वर्गीकृत करना है, जिनमें से प्रत्येक के अलग-अलग पारिस्थितिक कार्य हैं। कोर बड़े, अक्षुण्ण आवास हैं जो जैव विविधता और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। पुल और लूप, कोर या एक ही कोर के हिस्सों को जोड़कर कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। शाखाएँ कोर से निकलती हैं, जबकि किनारे उनकी सीमाओं को चिह्नित करते हैं। छिद्र कोर के भीतर की खाली जगहें हैं, और द्वीप छोटे, अलग-थलग पैच हैं।
अध्ययन में पाया गया है कि कोर क्षरण के प्रति सबसे अधिक लचीले होते हैं, जबकि द्वीप अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और तेजी से विखंडन की संभावना रखते हैं। द्वीपों पर हावी वनरोपण का पारिस्थितिक मूल्य न्यूनतम हो सकता है। प्रो. रामशंकरन ने मीडियाकर्मियों से कहा, ‘‘हमारी लचीलापन-आधारित रैंकिंग नीति निर्माताओं के लिए एक व्यावहारिक उपकरण प्रदान करती है। सभी वन क्षेत्रों को एक जैसा मानने के बजाय, यह यह पहचानने में मदद करती है कि कौन सी आकृतियाँ सबसे अधिक संवेदनशील हैं (जैसे द्वीप) और कौन सी दीर्घकालिक पारिस्थितिक मूल्य प्रदान करती हैं (जैसे कोर)।‘‘
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण या राष्ट्रीय हरित भारत मिशन जैसे वनरोपण कार्यक्रम मौजूदा कोर को मजबूत करने और उनके बीच पुल बनाने पर ध्यान केंद्रित करके लाभान्वित हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से बेहतर रूप से जुड़े हुए, अधिक लचीले और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ वन प्राप्त हो सकते हैं। इस ढाँचे में उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करके बुनियादी ढाँचे की योजना बनाने की भी क्षमता है जहाँ कनेक्टिविटी सबसे अधिक जोखिम में है, जिससे अधिक वैज्ञानिक रूप से सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है और पारिस्थितिक व्यवधान कम होता है।
रामशंकरन के अनुसार, ‘‘यह ढाँचा वन परिदृश्यों की संरचना का पता लगाने और उसे वर्गीकृत करने के लिए डैच्। नामक एक इमेज प्रोसेसिंग तकनीक पर निर्भर करता है।‘‘ अध्ययन के एक भाग के रूप में, शोधकर्ताओं ने कोपरनिकस ग्लोबल लैंड सर्विस (ब्ळस्ै) लैंड कवर मैप से प्राप्त 2015 से 2019 के वर्षों के लिए भारत के डिजिटल वन आवरण मानचित्रों पर विश्लेषण लागू किया। वन आवरण पर अधिकांश पिछले अध्ययनों के विपरीत,
इस अध्ययन में वन हानि और लाभ का अलग-अलग मानचित्रण किया गया है
‘‘परिणाम बताते हैं कि 2015 से 2019 तक, भारत के सभी राज्यों में वन क्षेत्र में शुद्ध हानि हुई। कुल मिलाकर, भारत में प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर वृद्धि के लिए 18 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का नुकसान हुआ। 56.3 वर्ग किलोमीटर सकल वन लाभ का लगभग आधा हिस्सा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान में हुआ, जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने मिलकर 1,032.89 वर्ग किलोमीटर सकल वन हानि का लगभग आधा हिस्सा प्राप्त किया,‘‘ अध्ययन में कहा गया है।
अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नए जोड़े गए आधे से अधिक वन क्षेत्र छोटे द्वीप हैं, जो संरचनात्मक संपर्क में पर्याप्त सुधार नहीं करते हैं। इससे पता चलता है कि जहाँ कागजों पर वन क्षेत्र बढ़ रहा है, वहाँ भी उन वनों का पारिस्थितिक मूल्य और लचीलापन सीमित हो सकता है। जहाँ तक अध्ययन के निहितार्थों का सवाल है, सत्यकुमार ने कहा, ‘‘हमारे परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि 2015-2019 के दौरान नए जोड़े गए अधिकांश वन छोटे-छोटे, अत्यधिक खंडित और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र थे। वर्तमान मात्रा-आधारित वनरोपण दृष्टिकोण से आगे बढ़ने और वन नियोजन में संरचनात्मक संपर्क को स्पष्ट रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।‘‘ यह भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की रिपोर्ट के बिल्कुल विपरीत है, जो वन आवरण में समग्र वृद्धि का संकेत देती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि एफएसआई ने वनों की पहचान के लिए सीजीएलएस से अलग मानदंडों का इस्तेमाल किया और खंडित तथा सतत वनों के बीच अंतर नहीं किया। एफएसआई वनाच्छादित क्षेत्रों को न्यूनतम 10 प्रतिशत वृक्ष छत्र आवरण वाले क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है और 23.5 मीटर रिजॉल्यूशन वाली उपग्रह छवियों पर निर्भर करता है। इसके विपरीत, इस अध्ययन में प्रयुक्त सीजीएलएस डेटासेट 15 प्रतिशत छत्र सीमा और 100 मीटर रिजॉल्यूशन लागू करता है।
हालांकि ये निष्कर्ष एफएसआई के निष्कर्षों से भिन्न प्रतीत होते हैं, जो अक्सर वन आवरण में समग्र वृद्धि का संकेत देते हैं, एफएसआई और इस अध्ययन के परिणाम सीधे तुलनीय नहीं हैं। एफएसआई वनों की पहचान के लिए सीजीएलएस से भिन्न मानदंडों का उपयोग करता है और खंडित तथा सतत वनों के बीच अंतर नहीं करता है। एफएसआई वनाच्छादित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है जहाँ न्यूनतम 10ः वृक्ष छत्र आवरण हो और यह 23.5 मीटर रिजॉल्यूशन वाली उपग्रह छवियों पर निर्भर करता है। इसके विपरीत, इस अध्ययन में प्रयुक्त सीजीएलएस डेटासेट 15ः छत्र सीमा और 100 मीटर रिजॉल्यूशन लागू करता है। शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सीजीएलएस डेटासेट पर भी निर्भर रहना पड़ा, क्योंकि इसी तरह के विश्लेषणों के लिए एफएसआई डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। सत्यकुमार ने कहा, ‘‘चूँकि एफएसआई रिपोर्टों में वन संपर्क आकलन शामिल नहीं होते हैं, इसलिए सीधी तुलना संभव नहीं है। हालाँकि, हमारे डेटा स्रोत की वैश्विक रूप से मान्य सटीकता 85ः से अधिक है, जिससे हमारे संपर्क परिणाम विश्वसनीय हैं। यदि एफएसआई का डेटा जीआईएस-संगत प्रारूप में उपलब्ध होता, तो हमारी कार्यप्रणाली को उस पर आसानी से लागू किया जा सकता था।‘‘
हालाँकि, वर्तमान अध्ययन की सीमाएँ भी हैं। उनमें से एक यह है कि 100 मीटर रिजॉल्यूशन पर, सड़कों और रेलमार्गों जैसी संकीर्ण रेखीय विशेषताओं का पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सकता है और 100 मीटर से छोटे वन खंड छूट सकते हैं। हालाँकि, इस ढाँचे की ताकत इसकी मापनीयता, लागत-प्रभावशीलता और ओपन-सोर्स टूल्स के उपयोग में निहित है। इससे बेहतर रिजॉल्यूशन पर समान डेटासेट के साथ सुसंगत परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है और इसे विभिन्न स्थानिक और लौकिक पैमानों पर लागू किया जा सकता है। प्रोफेसर रामशंकरन ने कहा, ‘‘हमारा ढाँचा जिलों या संरक्षित क्षेत्रों जैसे बेहतर पैमानों पर पूरी तरह से विस्तार योग्य है, और इसका उपयोग सड़कों और रेल लाइनों जैसे रेखीय बुनियादी ढाँचे के वन संपर्क पर पड़ने वाले प्रभावों का अधिक केंद्रित तरीके से विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। यह इसे भारत और वैश्विक स्तर पर समान संदर्भों में, वन क्षेत्रों में और उसके आसपास दीर्घकालिक वन निगरानी, योजना और सूचित बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए एक मूल्यवान उपकरण बनाता है।‘‘
शोधकर्ता वन विखंडन के स्थानीय कारणों का अध्ययन करने और वर्तमान संरक्षण एवं वनीकरण प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए अपने ढाँचे को और विकसित करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि रिपोर्ट में वन आवरण में वृद्धि में योगदान देने वाले वनों की गुणवत्ता को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, न ही वन क्षरण के कारणों पर डेटा प्रदान किया गया है, आईआईटी बॉम्बे के अध्ययन से भारत में वन विखंडन और क्षति को संबोधित करने और संरक्षण के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता का संकेत मिलता है।















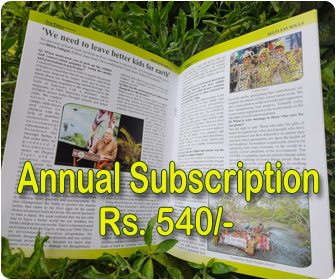
Leave a comment