Green Business
जैवविविधता संरक्षण की ओरः सरयू किनारे महिलाओं का हस्तशिल्प अभियान
उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले के चाइनपुरवा गाँव में सरयू नदी के तट पर रहने वाले मछुआरा समुदाय का जीवन लंबे समय से नदी की मछलियों पर निर्भर रहा है। हालाँकि, हाल के वर्षों में प्रकृति संरक्षण तथा टिकाऊ विकास की आवश्यकता ने उन्हें अपनी आजीविका के लिए नए रास्ते खोजने पर विवश किया है। इसी कड़ी में, टीएसए इंडिया फाउंडेशन के इंडियन टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम के सहयोग से गाँव की महिलाओं ने जलकुंभी जैसी आक्रामक, अनुपयोगी समझी जाने वाली जल-वनस्पति को अपनी शक्ति बनाकर हस्तशिल्प निर्माण का सफल व्यवसाय खड़ा किया है।
पारंपरिक मछली पकड़नाः एक संकट और उसकी चुनौती
सरयू की मछलियाँ और जलीय जीव, विशेषकर वहाँ पाए जाने वाले नौ प्रजातियों के मीठे पानी के कछुए, नदी की जैव-विविधता के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। परंतु मत्स्याखेट पर अत्यधिक निर्भरता ने इस पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल दिया था। असंयमित मत्स्याखेट ने न केवल मछली और कछुओं की संख्या कम की, बल्कि उनके प्रजनन केंद्रों को भी प्रभावित किया, जिससे नदी की प्राकृतिक पुनरुत्पादन क्षमता कम हो रही थी।
हरित विकल्पः जलकुंभी हस्तशिल्प से रोजगार
जलकुंभी सामन्यतः एक हानिकारक खर-पतवार के रूप में जानी जाती है, जो जल स्रोतों को अवरुद्ध कर देती है और जलीय जीवन को बाधित करती है। लेकिन टीएसए इंडिया फाउंडेशन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में गाँव की महिलाओं ने जलकुंभी से चटाई, टोकरियाँ, बैग व अन्य सजावटी व उपयोगी उत्पाद बनाना सीखकर इसे आजीविका का साधन बना दिया। यह पहल न केवल पर्यावरण की सफाई है, वरन् स्थानीय हुनर के संवर्धन और आत्मनिर्भरता का भी माध्यम है।
जैव-विविधता संरक्षण और संवेदनशील नदी क्षेत्र
मछुआरों से मछली पकड़ने के बजाय अन्य रोजगार तलाशने की अपील करना तब तक प्रभावशाली नहीं होता जबतक आप उन्हें आजीविका का कोई अतिरिक्त साधन उपलब्ध न करा दें। मछुआरा समुदाय के द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प को यदि बाजार में जगह और अच्छा मूल्य मिले तो मछुआरा समुदाय को मछली मारने के स्थान पर नदी व उसके जैवतंत्र के संरक्षण में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकता है। हस्तशिल्प का यह नया रास्ता महिलाओं को आमदनी देता है, साथ ही समुदाय के अन्य सदस्यों को भी संवेदनशील इलाकों में मत्स्याखेट छोड़ने की प्रेरणा देता है। जैव-विविधता के संरक्षण के इस प्रयास से नदी में कछुओं का प्रजनन चक्र अब व्यवधान-रहित हो रहा है।
इको-फ्रेंडली उत्पादः स्थानीय और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए वरदान
जलकुंभी से बने उत्पाद 100ः बायोडिग्रेडिबल व प्राकृतिक होते हैं, जिनमें कोई रसायन अथवा प्लास्टिक नहीं होता। इससे पर्यावरण में अधिशेष अपशिष्ट या प्रदूषण नहीं फैलता। इसके अलावा, जलकुंभी हटाने से नदी की जल-गुणवत्ता बढ़ती है और स्थानीय भू-जल व पारिस्थितिक संतुलन भी कायम रहता हैकृयही सच्ची ‘ग्रीन अर्थव्यवस्था’ की मिसाल है।
बाजार और स्वावलंबन
गाँव की महिलाओं के द्वारा बनाए गए जलकुंभी हस्तशिल्प स्थानीय संतोष ढाबा पर बेंचा जा रहा है, जिससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ी है बल्कि पर्यावरण-मित्र उत्पादों की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। हर खरीदार को पता चलता है कि उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु प्रकृति, कछुओं और नदी के स्वास्थ्य को भी बचा रही है। हालांकि अभी भी उन उत्पादों को बेंचना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है क्योंकि लोग प्लास्टिक के सस्ते सामान ही खरीदना चाहते हैं। लेकिन सभी के प्रयासों से यदि इन उत्पादों को बाजार में उचित स्थान मिले तो ये अभियान और अधिक सफल बनेगा और अन्य ग्रामवासियों के लिए भी एक मॉडल होगा।
हरित कारोबार की सीख
यह कहानी केवल ग्राम्य भारत की महिलाओं की नहीं, बल्कि सामुदायिक नेतृत्व और पर्यावरण-मानव सहअस्तित्व का भी प्रतीक है। जब सही प्रशिक्षण, सहयोग और विकल्प उपलब्ध हो, तब वंचित व सीमांत समुदाय भी जैव-विविधता संरक्षण में अग्रसर हो सकते हैं। चाइनपुरवा गाँव की महिलाएँ आज इको-फ्रेंडली हरी अर्थव्यवस्था की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रही हैं, जहाँ पर्यावरण हितैषी आजीविका, आत्मबल और प्रकृति संरक्षण का सुंदर संगम संभव हुआ है।
(Interviewed by Abhishek Dubey, President, Nature Club Foundation, Gonda, UP)















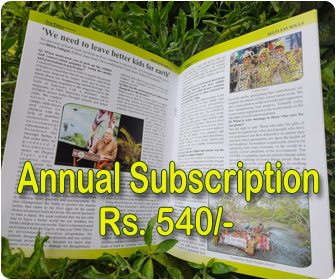
Leave a comment