Specialist's Corner
प्रशान्त कुमार वर्तमान में उत्तराखण्ड वन विभाग में वरिष्ठ परियोजना सहयोगी(वन्यजीव) के पद पर कार्यरत हैं तथा पिछले सात वर्षों से वन्यजीव अपराध नियंत्रण एवं संरक्षण में प्रभावी शोध एवं विश्लेषण कार्य कर रहे है। इन्होंने लगभग पन्द्रह हजार से अधिक वन कर्मियों को वन्यजीव फॉरेंसिक एवं वन्यजीव संरक्षण विषय में प्रशिक्षित किया है तथा पांच सौ से अधिक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है। कुमार, फॉरेंसिक विज्ञान में बीएससी तथा एमएससी है एवं वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक्स में फील्ड के अनुभवी हैं।
भारत सहित दुनियाभर में वन्यजीवों की अवैध तस्करी, शिकार और अंगों के व्यापार जैसी आपराधिक गतिविधियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। ये अपराध न केवल जैव विविधता को खतरे में डालते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन पर भी गंभीर प्रभाव डालते हैं। इन जघन्य अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जहां एक ओर सख्त कानून बनाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर फॉरेंसिक तकनीक अब अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने में एक क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है। वन्यजीव अपराधों में शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार जैसे कृत्य शामिल होते हैं, जो दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत जैसे जैव- विविधता से भरपूर देश में यह समस्या और भी गंभीर है। बाघ, हाथी, तेंदुआ, कछुए, दुर्लभ पक्षी और यहां तक कि छोटी-छोटी प्रजातियाँ भी इस आपराधिक जाल का शिकार बन रही हैं। ये अपराध केवल किसी एक जानवर की जान लेने तक सीमित नहीं हैं। जब किसी प्रजाति की संख्या कम होती है या वह विलुप्त होने लगती है, तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) की संतुलन बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बाघ जैसे शिकारी जानवर कम हो जाते हैं, तो शाकाहारी जानवरों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ सकती है, जिससे जंगल की हरियाली और अन्य प्रजातियाँ प्रभावित होती हैं। इसका असर अंततः मनुष्य पर भी पड़ता है। पानी के स्रोतों पर दबाव, खेती की समस्याएँ और जलवायु असंतुलन इसके उदाहरण हैं। वन्यजीव अपराधों की रोकथाम में पारंपरिक विधियों के साथ-साथ अब फॉरेंसिक तकनीकों की भूमिका बेहद अहम हो गई है। आइए जानें कि ये आधुनिक तकनीकें वन्यजीव अपराधों की जांच में कैसे काम करती हैं -
1. डीएनए विश्लेषणः पहचान का वैज्ञानिक तरीका
जब वन्यजीव अपराध की जांच की जाती है, तो अपराध स्थल या तस्करों के पास से अक्सर केवल अवशेष ही मिलते हैं-जैसे खाल, हड्डी, सींग, पंख, बाल या मांस। कई बार ये अवशेष इतने टूटे-फूटे या बदले हुए रूप में होते हैं कि सिर्फ देखने से यह बताना मुश्किल हो जाता है कि वे किस जानवर के हैं। ऐसे मामलों में डीएनए विश्लेषण एक भरोसेमंद और वैज्ञानिक तरीका बनकर सामने आता है।
फॉरेंसिक विशेषज्ञ इन अवशेषों से सूक्ष्म स्तर पर डीएनए निकालते हैं और फिर उसे प्रयोगशाला में उस जानवर की ज्ञात प्रजातियों के डीएनए से मिलाते हैं। यह तकनीक न केवल यह साबित करती है कि अवशेष किस जानवर से संबंधित हैं, बल्कि कई बार यह भी पता लगाया जा सकता है कि वह जानवर किस इलाके में पाया जाता है(ज्योग्राफिकल ओरिजिन), उसका नर या मादा होना, वह पालतू है या जंगली, उसके माता-पिता के बारे में जानकारी और क्या वह किसी संरक्षित प्रजाति से संबंधित था।
उदाहरणः
अगर किसी तस्कर के पास से खाल बरामद की जाती है और वह दावा करता है कि वह किसी सामान्य जानवर की है, तो डीएनए जांच से यह स्पष्ट रूप से साबित किया जा सकता है कि वह खाल बाघ की है, और इस तरह तस्कर के झूठ का पर्दाफाश होता है। यह तकनीक अदालत में सबूत के तौर पर भी बेहद शक्तिशाली मानी जाती है क्योंकि यह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है, अनुमान या मान्यता पर नहीं।
वन्यजीव फॉरेंसिक में मल (स्कैट या फेसेस) से डीएनए निकालना आज एक बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी तकनीक बन गई है, खासकर तब जब जानवर को सीधे पकड़ना या उसके शरीर के हिस्से प्राप्त करना संभव नहीं होता। आइए सरल भाषा में समझते हैं-
मल से डीएनए कैसे निकाला जाता है?
जब कोई जानवर मल त्याग करता है, तो उस मल में सिर्फ अपशिष्ट नहीं होता, उसमें जानवर की आंतरिक कोशिकाएं, आंतों के माइक्रोबायोम, और कई बार खून, त्वचा या आंतरिक कोशिकाओं के अंश भी होते हैं। इन्हीं से वैज्ञानिक डीएनए निकाल सकते हैं।
प्रक्रियाः
सैंपल कलेक्शनः मल को साफ, सूखे और प्रदूषण-मुक्त तरीके से जंगल में एकत्र किया जाता है। इसे विशेष रूप से तैयार किये गए डीएनए संरक्षक रसायनों में रखा जाता है ताकि डीएनए खराब न हो।
डीएनए एक्सट्रैक्शनः मल को लैब में लाकर उसमें से कोशिकाओं को अलग किया जाता है। विशेष रसायनों की मदद से इन कोशिकाओं का डीएनए निकाला जाता है।
पीसीआर और विश्लेषणः डीएनए की मात्रा कम होने के कारण उसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक से कई गुना बढ़ाया जाता है ताकि उसे पढ़ा जा सके। इसके बाद जीन की तुलना रेफरेंस डीएनए से की जाती है।
पहचान (स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन)ः प्राप्त डीएनए को डेटाबेस से मिलाकर यह तय किया जाता है कि वह किस प्रजाति का है जैसे बाघ, तेंदुआ, भालू, आदि।
क्यों उपयोगी है ये तकनीक?
ऽ जानवर को देखे बिना भी उसकी उपस्थिति का पता चलता है।
ऽ इससे वन्यजीवों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है।
ऽ अपराध के मामलों में यह साबित किया जा सकता है कि इलाके में कौन-सी प्रजाति मौजूद थी।
ऽ यह पूरी तरह नॉन-इन्वेसिव यानी बिना जानवर को नुकसान पहुंचाए की जाने वाली तकनीक है।
कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र और इसके एक विशेष भाग लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण प्रयोगशाला हैदराबाद स्थित एक अत्याधुनिक जैवविज्ञान संस्थान है, जो भारत सरकार के कॉउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत कार्य करता है। यह संस्थान संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण और वन्यजीव फॉरेंसिक जांच में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2. सूक्ष्म साक्ष्य बाल, पंख और खाल की जांच
वन्यजीव अपराधों की जांच में कभी-कभी अपराधी कोई बड़ा सबूत नहीं छोड़ते, लेकिन उनके पीछे छूटे हुए बाल, पंख या खाल के छोटे-छोटे टुकड़े भी बहुत कुछ कह सकते हैं। ये अवशेष देखने में साधारण और महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन एक प्रशिक्षित फॉरेंसिक विशेषज्ञ के लिए ये ‘‘क्राइम सीन‘‘ के सबसे महत्वपूर्ण सुराग साबित हो सकते हैं। इन साक्ष्यों की जांच के लिए अत्याधुनिक माइक्रोस्कोपिक तकनीकों और विशेष लैब परीक्षण (जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, किरेटिन विश्लेषण आदि) का प्रयोग किया जाता है। इनसे यह पता लगाया जा सकता है कि बाल या पंख किस प्रजाति से हैं, जानवर की उम्र कितनी थी, और यहां तक कि वह स्वस्थ था या बीमार।
यह तकनीक खासतौर पर उपयोगी है जबः
ऽ किसी पक्षी के पंख से उसकी दुर्लभ या संरक्षित प्रजाति की पहचान करनी हो।
ऽ छोटे स्तनधारी जानवरों (जैसे ऊदबिलाव, गिलहरी, लोमड़ी आदि) की तस्करी या शिकार के मामले में सटीक साक्ष्य जुटाने हों।
ऽ केवल खाल का एक छोटा हिस्सा मिलने पर प्रजाति की पुष्टि करनी हो।
भारत में वन्यजीव अपराधों की जांच में सलीम अली सेंटर फॉर ओर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री एक अग्रणी संस्था है, जो विशेष रूप से पक्षियों से जुड़े अपराधों की जांच में फेदर मॉर्फोमेट्रिक्स तकनीक का उपयोग करती है। फेदर मॉर्फोमेट्रिक्स एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें पंखों के आकार, लंबाई, चैड़ाई, वक्रता और बनावट का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। यह विधि खासतौर पर तब कारगर होती है जब किसी पक्षी के केवल पंख या पंखों के टुकड़े मिलते हैं और बाकी शरीर उपलब्ध नहीं होता। सैकोन के विशेषज्ञों के पास एक विस्तृत फेदर रेफरेंस कलेक्शन है, जिसमें सैकड़ों पक्षी प्रजातियों के पंखों के माप और विशेषताएं दर्ज हैं। जब किसी अपराध स्थल से पंख बरामद होते हैं, तो उन्हें सैकोन भेजा जाता है, जहाँ पंखों के मॉर्फोलॉजिकल माप लिए जाते हैं। उनके रंग, बनावट, और मापदंडों की तुलना रेफरेंस डेटाबेस से की जाती है। इस तुलना से यह निर्धारित किया जाता है कि पंख किस प्रजाति के हैं जैसे मोर, चील, उल्लू, बाज आदि।
फॉरेंसिक जांच में उपयोगिताः
यह तकनीक खासतौर पर उल्लुओं की अवैध तस्करी में बेहद उपयोगी साबित हुई है, क्योंकि भारत में उल्लुओं का इस्तेमाल काले जादू जैसी गतिविधियों में किया जाता है।पक्षियों के पंखों से बने शृंगार या धार्मिक वस्तुओं की वैधता जांचने में भी इस तकनीक की मदद ली जाती है।
3. फॉरेंसिक नेक्रोप्सीः मौत की वजह जानना
जब जंगल या किसी संरक्षित क्षेत्र में किसी वन्यजीव की लाश (कारकस) पाई जाती है, तो यह जरूरी होता है कि उसकी मौत के कारणों की सटीक जांच की जाए। ऐसे मामलों में की जाती है वाइल्डलाइफ नेक्रोप्सी (जिसे पोस्ट-मॉर्टम एग्जामिनेशन भी कहते हैं) । यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रशिक्षित वन्यजीव पशु चिकित्सक (वाइल्डलाइफ वेटेरिनरियन) और फॉरेंसिक विशेषज्ञ जानवर के शरीर की गहन जांच करते हैं।
नेक्रोप्सी के दौरान देखे जाने वाले मुख्य बिंदुः
ऽ बाहरी चोटें (एक्सटर्नल इंजरीज)ः क्या शरीर पर कोई गोली का निशान है? या धारदार हथियार से हमला हुआ है?
ऽ भीतरी अंगों की स्थितिः अंगों में सूजन, फटाव, रक्तस्राव आदि से जहर या अंदरूनी चोट का संकेत मिल सकता है।
ऽ जहर के संकेतः यदि जानवर ने कोई जहरीला पदार्थ खाया है, तो उसके पेट या आंतों से नमूने लेकर लैब में जांच की जाती है।
ऽ गला घोंटना या फंदाः कई बार जानवर को फंदे में फँसा(स्नेरिंग) कर मारा जाता है। गले पर निशान या त्वचा की टूट-फूट इसका संकेत देती है।
ऽ शव का विघटन स्तरः मौत कितनी देर पहले हुई इसका अनुमान लगाया जाता है, जो अपराध के समय और संदिग्ध की पहचान में मदद करता है।
4. ट्रॉफी फॉरेंसिकः अवैध व्यापार का भंडाफोड़
वन्यजीव अंगों से बनी ‘‘ट्रॉफियां‘‘ जैसे बाघ की खाल, हाथी के दांत (आइवरी), गैंडे का सींग, हिरण की सींग, या भालू के पंजे अक्सर अवैध वन्यजीव तस्करी का केंद्र होती हैं। इनका इस्तेमाल गहनों, सजावट, या अंधविश्वासी उत्पादों में किये जाने के कारण ही इनका व्यापर किया जाता है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा इन ट्रॉफियों का विश्लेषण करके अपराधियों तक पहुँचते है।
ट्रॉफी फॉरेंसिक में विशेषज्ञ इन ट्रॉफियों पर मौजूदः
ऽ डीएनए अवशेष (जैसे खाल के अंदरूनी हिस्सों से त्वचा के टुकड़े),
ऽ बाल या ऊतक के अंश,
ऽ कट के निशान (किस औजार से काटा गया), और
ऽ रासायनिक अवशेष (जैसे संरक्षक रसायन, गोंद, रंग आदि) का गहन परीक्षण करते हैं।
ये जांच यह साबित कर सकती है किः
ऽ ट्रॉफी किस जानवर की है,
ऽ वह जानवर कहां पाया गया था (जेनेटिक ओरिजिन) और
ऽ ट्रॉफी को किस औजार से तैयार किया गया, जिससे संभावित अपराधी की पहचान हो सके।
उदाहरण के लिए, अगर किसी के घर से बाघ की खाल बरामद होती है, तो डीएनए टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि वह खाल किस रिजर्व से गायब हुए बाघ की है। इससे शिकार, तस्करी और बाजार नेटवर्क का खुलासा होता है। ट्रॉफी फॉरेंसिक न केवल एक जानवर की पहचान में मदद करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय तस्करी रैकेट, क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क, और अवैध बाजारों को भी उजागर करने में अहम भूमिका निभाता है। यह तकनीक कानून को अपराधियों के और करीब ले जाती है भले उनके पास केवल एक खाल ही क्यों न हो।
5. डेटा और डिजिटल फॉरेंसिकः नेटवर्क का पर्दाफाश
आजकल अवैध वन्यजीव व्यापार केवल जंगलों या सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर भी इसका तेजी से फैलाव हो रहा है। अपराधी अब बाघ की खाल, दुर्लभ पक्षियों, या गैंडे के सींग जैसे अवैध उत्पादों की डीलिंग फेसबुक, व्हाट्सप्प, टेलीग्राम, और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर करने लगे हैं। इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड को उजागर करने के लिए आज डिजिटल फॉरेंसिक तकनीकें बेहद जरूरी हो गई हैं।
डिजिटल फॉरेंसिक में विशेषज्ञ निम्नलिखित चीजों का विश्लेषण करते हैंः
ऽ मोबाइल डेटा एनालिसिसः कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड(सीडीआर), सेल आईडी, चैट हिस्ट्री, ब्राउजिंग डेटा से जुड़ी जानकारी निकाली जाती है।
ऽ ईमेल और सोशल मीडिया ट्रैकिंगः ईमेल एक्सचेंज, सोशल पोस्ट, और प्राइवेट ग्रुप चैट्स को ट्रेस किया जाता है।
ऽ जीपीएस और लोकेशन डेटाः संदिग्धों की लोकेशन हिस्ट्री से यह पता चलता है कि वे वन्यजीव क्षेत्रों में कब गए थे।
ऽ डार्क वेब निगरानीः कई अपराधी दुर्लभ प्रजातियों का व्यापार डार्क वेब के जरिए करते हैं। इसे ट्रैक करने के लिए विशेष टूल्स का प्रयोग होता है।
डिजिटल फॉरेंसिक अब वन्यजीव अपराध रोकथाम का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह न केवल अपराध की पुष्टि करता है, बल्कि अपराधियों के नेटवर्क, पैटर्न, और लोकेशन का भी पर्दाफाश करता है। आज का अपराधी चाहे जंगल में छिपा हो या मोबाइल स्क्रीन के पीछे डिजिटल तकनीकें उसे ढूंढ़ निकालने में सक्षम हैं।
6. मानव-वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीव फॉरेंसिक की भूमिका
आज भारत के कई हिस्सों में जंगल और बस्तियों की सीमाएं आपस में घुलने लगी हैं। बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू जैसे जंगली जानवर अक्सर खेतों, गांवों या कस्बों में पहुंच जाते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष (ह्यूमन-वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट) की घटनाएं बढ़ रही हैं। कभी इंसान घायल होता है, कभी पशु मारे जाते हैं, और कई बार वन्यजीवों की मौत या गायब होना शिकार के शक को जन्म देता है। ऐसे हालात में वन्यजीव फॉरेंसिक एक बेहद जरूरी भूमिका निभाता है। यह तय करता है कि घटना प्राकृतिक थी, रक्षा में की गई हत्या थी, या जानबूझकर की गई क्रूरता या तस्करी से जुड़ी हुई थी।
मानव-वन्यजीव संघर्ष के केस में फॉरेंसिक कैसे मदद करता है?
हमले की सच्चाई जाननाः अगर कोई व्यक्ति घायल होता है या मारा जाता है, तो उसके शरीर से लिए गए घावों, बालों, कपड़ों पर मौजूद निशानों की जांच कर यह साबित किया जा सकता है कि हमला किस जानवर ने किया बाघ, तेंदुआ, भालू या कुछ और? डीएनए सैंपल (नाखून, दांत के निशान, लार) से जानवर की पहचान की जा सकती है।
प्रतिशोध में हत्या या शिकार की पुष्टिः अक्सर जानवरों को बिजली के तार, जहर, या फंदे से मार दिया जाता है। जब कोई बाघ मरा पाया जाता है, तो फॉरेंसिक नेक्रोप्सी बताती है कि उसकी मौतः
ऽ इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई,
ऽ जहर देकर मारा गया,
ऽ या किसी मानव हमले का शिकार हुआ।
पशु-पशु संघर्ष या मानव हस्तक्षेपः कभी-कभी दावा किया जाता है कि दो बाघों की लड़ाई में एक मरा, लेकिन फॉरेंसिक जांच (जैसे दांत के निशान, डीएनए, घाव की प्रकृति, आसपास की झाड़ियों का टूटना) से ये साबित हो सकता है कि उसकी मौत मानव द्वारा की गई थी, ना कि आपसी संघर्ष से।
मुआवजे की प्रक्रिया में प्रमाणः मानव-वन्यजीव संघर्ष में सरकार मुआवजा देती है, लेकिन कई बार झूठे दावे भी सामने आते हैं। फॉरेंसिक जांच यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि हमला वाकई किसी वन्यजीव द्वारा हुआ था।
रिपीट ऑफेंडर की पहचानः कई बार एक ही बाघ या तेंदुआ बार-बार गांवों में घुसता है और हमला करता है। फॉरेंसिक डीएनए से यह पता लगाया जा सकता है किः
ऽ क्या हर बार हमला एक ही जानवर ने किया?
ऽ क्या यह बाघ पहले किसी केस में शामिल था?
इससे ट्रैकिंग और ट्रांसलोकेशन (स्थानांतरण) की योजना बनाई जा सकती है।
डेटा संग्रह और नीति निर्माणःवन्यजीव फॉरेंसिक से इकट्ठा किए गए डेटा (डीएनए प्रोफाइल, संघर्ष की प्रवृत्ति, प्रजाति आधारित व्यवहार) का उपयोगः
ऽ पॉलिसी बनाने,
ऽ जोखिम क्षेत्र की पहचान,
ऽ और सुरक्षा उपाय तय करने में किया जाता है।
मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं अक्सर भावनात्मक, संवेदनशील और कानूनी रूप से जटिल होती हैं। ऐसे में वन्यजीव फॉरेंसिक ही वह वैज्ञानिक विधा है जोः
ऽ सच्चाई की परतें खोलता है,
ऽ निर्दोषों को बचाता है,
ऽ और अपराधियों को न्याय के कटघरे तक ले जाता है।
यह तकनीक केवल अपराध पकड़ने का साधन नहीं, बल्कि वन्यजीवों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिशा में एक अहम कदम है। मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसे संवेदनशील मामलों में फॉरेंसिक तकनीकें सच्चाई तक पहुँचने का सबसे निष्पक्ष और वैज्ञानिक रास्ता हैं। यह न केवल बेकसूर इंसानों को न्याय दिलाने में मदद करता है, बल्कि वन्यजीवों को बेवजह मारे जाने से भी बचाता है, और अपराधियों को चिन्हित करता है।
कुछ प्रमुख केस उदाहरणः
हत्था जोड़ी का अवैध व्यापारः अंधविश्वास, तस्करी और वन्यजीव फॉरेंसिक की कहानी
तमिलनाडु के उन्नत वन्यजीव संरक्षण संस्थान में वन्यजीव फोरेंसिक विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिको ने बंगाल मॉनिटर लिजार्ड के संसाधित नर गोनाड की अवैध तस्करी एवं बिक्री का पर्दाफांश किया था। इस केस में पकडे गए वन्यजीव उत्पाद को शिकारियों द्वारा मार्टिनिया एनुआ की जड़ों की आड़ में बेचे जाने वाले सूखे पशु अंग वास्तव में बंगाल मॉनिटर छिपकलियों के संसाधित नर गोनाड थे जिसे हथा जोड़ी कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने डीएनए परीक्षण के आधार पर साबित किया कि बरामद उत्पाद किसी पौधे कि जड़ न होकर वन्य जंतु बंगाल मॉनिटर छिपकलियों का आंतरिक प्रजनन अंग है। इस खुलासे के कारण तमिलनाडु में उन शिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, जिन्होंने अवैध पशु अंगों को पौधों की सामग्री के रूप में झूठ बोलकर बेचा जा रहा था।
सफेद गैंडा ‘कैंपबेल‘ की हत्या और वन्यजीव फॉरेंसिक की निर्णायक भूमिका
कैंपबेल, एक सफेद गैंडा, दक्षिण अफ्रीका के एक निजी वन्यजीव रिजर्व में वर्षों से सुरक्षित जीवन जी रहा था। लेकिन वह एनडलोवू गिरोह एक कुख्यात वन्यजीव शिकारी समूह के आखिरी शिकार का शिकार बना। गैंडे के सींगों की भारी मांग, विशेषकर एशियाई काले बाजारों में (जहाँ इसे औषधीय या प्रतीकात्मक मूल्य के साथ जोड़ा जाता है), इस गिरोह को अत्यंत संगठित और खतरनाक बना चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद, तीनों आरोपी ग्राहमस्टाउन के मकाना रिजॉर्ट में गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके पास से जो वस्तुएं बरामद कीं, वे बेहद आपराधिक थींः
ऽ धनुष से चलने वाली आरी,
ऽ ट्रैंक्विलाइजर डार्ट गन (बेहोशी की बंदूक),
ऽ ताजा निकाला गया गैंडे का सींग, और
ऽ सींग व आरी पर लगा खून।
डीएनए फॉरेंसिक की निर्णायक भूमिकाः
डीएनए फॉरेंसिक वह मोड़ था, जिसने आरोपियों को सीधे कैंपबेल की हत्या से जोड़ा। गैंडे के सींग पर मिले ऊतक और खून के नमूनों का मिलान किया गया। आरी पर लगा खून और ऊतक भी डीएनए के लिए जांचा गया। इन नमूनों की तुलना कैंपबेल के संरक्षित डीएनए प्रोफाइल से की गई। पूरा मेल यह साबित करता है कि वही सींग कैंपबेल का था और वही औजार उसकी हत्या में प्रयोग हुआ। प्रिटोरिया विश्वविद्यालय की सिंडी हार्पर, जो एक पशु आनुवंशिकी विशेषज्ञ हैं, ने इस मामले में निर्णायक भूमिका निभाई। इस केस ने दुनिया को दिखाया कि कैसे वन्यजीव फॉरेंसिक, विशेष रूप से डीएनए तकनीक, सिर्फ संरक्षण नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण का भी अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। कैंपबेल की मृत्यु केवल एक गैंडे की हत्या नहीं थी, यह एक पूरी जैव विविधता प्रणाली पर हमला था। लेकिन विज्ञान और फॉरेंसिक की मदद से, न केवल अपराधी पकड़े गए, बल्कि यह भी साबित हुआ कि-
‘‘प्राकृतिक दुनिया को बचाने के लिए हमें कानून, विज्ञान और संवेदनशीलता तीनों की एकजुट ताकत की जरूरत है।‘‘















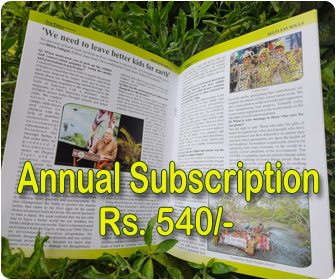
Leave a comment